‘ विद्यार्जन के लिए विद्यालय कितने
जरूरी ’ – देश , काल और परिस्तिथि की आधारशिला पर एक समग्र चिंतन
आलेख द्वारा अमित तिवारी ; सहायक प्राध्यापक- पर्यटन प्रबन्ध
भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संसथान , ग्वालियर म. प्र.
(पर्यटन मंत्रालय के अधीन एक संगठन)
भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले विकासशील देश में जहाँ अनेकानेक
चुनौतियाँ – ग़रीबी , अपराध ,अशिक्षा , असमता , आतंरिक उठापटक व अन्योन्य आर्थिक
आधारित गतिविधियों पर आधारित अर्थव्यवस्था ; जिसमे 8 % की वार्षिक विकासदर प्राप्त
होना अथवा सुचारू रहना महती आवश्यकता होती है I ऐसे राष्ट्र में स्कूल आधारित
प्रारंभिक शिक्षा देश की बुनियादी आवश्यकता और उसके प्रकटन द्वारा सैद्धांतिक तौर
पर ; समूचे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का मूल धेय्य तय किया जाता है I यहाँ यह
नितांत आवश्यक है की हम समझें की देश की शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा , माध्यमिक
शिक्षा व सेकेंडरी शिक्षा केन्द्रों के तौर पर विद्यालय या की स्कूल कितने
महत्त्वपूर्ण केंद्र होतें हैं I बिना ज्ञान के जीवन का धेय्य नीरस है और ज्ञान की
परिपाटी बच्चे को मनुष्य रूप में माँ के इर्द-गिर्द से मिलती है I इसके उपरांत
उसका विकास क्रमशः – शब्द निबंधन, वाक्य विन्यास, भावना बोध और विषयगत बोध को धारण
करने की प्रक्रिया से गुजरता है जहाँ उसके तेजी से बदलते मष्तिष्क को ज्ञान आधारित
प्रक्रियाओं और अनुशासन आधारित सीमाओं की आवश्यकता ऐसी व्यवस्था से पूरी होती है ;
जहाँ उसके ज्ञान की भूख और अनुशासित हो तदर्थ शारीरिक , मानसिक रूप से परिपक्व हो
एक विषय विशारद हो पाने की ललक मूर्त रूप ले पाती है I इसमें राष्ट्रधर्म,
राज धर्म , शरीर धर्म , समाज धर्म और परिवार धर्म महत्वपुर्ण लक्ष्यों को हांसिल
करने के गुणों की शिक्षा बालक को प्राप्त होती है I भारतीय परिदृश्य में तो यह
इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन मूल्यों आधारित भारतीय समाज में इसका पल्लवन
विद्यालयों के माध्यम से होता है ;और इसे विद्या अर्जन के केंद्र के तौर पर एक
मंदिर सम पवित्रता की समता भी दी गयी है I जैसे
जीवन में आध्यात्मिकता के केंद्र के तौर पर सनातनी भारतीय परंपरा में
मंदिरों की प्रासंगिकता रही है और उसे स्थापित करने का विज्ञान भारतीयता में अनंतकाल
से चला आया है I उसी तरह से विद्यार्जन के केन्द्रों के तौर पर इसकी सार्थकता व
प्रासंगिकता हमेशा ही विद्यमान रही है I यद्यपि बदले परिदृश्य में कुछेक भ्रामक
स्तिथियाँ विद्या केन्द्रं यानि विद्यालयों के परिपेक्ष्य में भी बदलें हाल में
परिवर्तित हुयी हैं , जिन्हें देश काल और परिस्थितियों के बदले स्वरुप में देखना
बहुत महत्त्वपूर्ण होता है I हालाँकि कालांतर में आये कुछ आमूल – चूल परिवर्तनों
के द्वारा समाज व राष्ट्र हित में विद्यालयों की भूमिका बदली है; हरेक परिवर्तन
हमेशा प्रभावी व सकारात्मक नहीं होता ; किन्तु कई बार विडंबनाओं से भरपूर भी हो
जाता है I
देश की समग्र कल्पना यदि यदि युवा पीढ़ी के बिना
या उनके समग्र विकास के बिना हो जाये तो शायद इन केन्द्रों(विद्यालयों ) की भूमिका
भी इतनी महत्त्वपूर्ण न भी हो ; लेकिन इस तथ्य को भी झुठलाना यकीनन असंभव है की
भारतीयता में; या कि देश की दशा- दिशा तय करने में शिक्षा व शिक्षा आधारित सर्जनशील
समाज जिससे समग्र राष्ट्र की सकारात्मक अर्थ नीति का धेय्य रचा जाता है; अत्यंत
महत्त्वपूर्ण होती है I रामचरितमानस जो कि जनमानस व समाज का समग्र कालजयी दर्पण
रहा है , में महाकवि द्वारा विद्यालयों की आवश्यकता को उदृत करते हुए लिखा है –
“गुरु गृह पढ़न चलेहु
रघुराई I अल्प कालविद्या सब आई II ”
इस कालजयी रचना के माध्यम से युग –युगांत में विद्यार्जन के लिए
विद्यालय /गुरुकुल आदि की महत्ता को वर्णित किया गया है , लेकिन बदले हुए परिदृश्य
में भी शिक्षा की समग्र आवश्यकता के मूल के शुभारम्भ के वितान को विद्यालयों
द्वारा ही गढ़ा जाता रहा है I महत्त्वपूर्ण है की शब्द ज्ञान से होते हुए सत्य के
बोधन और समग्र विश्व की व्यष्टि को समझने का वितान गढ़ती विद्यालयीन शिक्षा एक
महत्त्वपूर्ण प्रकल्प है ; जिसमे ज्ञान आधारित संश्लेषण और समन्वय आधारित विश्लेषण
द्वारा पीढ़ियों की एक समग्र समता और वैज्ञानिकता का अति विशेष पाठ पढ़ाया जाता है I
बदले हुए परिदृश्य में कालांतर में भी राष्ट्रवाद के विकास और राष्ट्रीय
आन्दोलन को बदल देने में विद्यालयों या की
विद्यार्जन केन्द्रों की अति विशेष भूमिका परिलक्षित हुयी है I समय के समकक्ष
व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बना उसके द्वारा समाज व प्रकृति हित हेतु नित नवीन
अनुसन्धान वृत्ति का सृजन कालक्रम में भारतीय पुनर्जागरण युग में आये एक शून्यवाद
के प्रतिकार के तौर पर पैदा हुआ; जिसमे बदले हुए परिदृश्यों में कुछ परिवर्तन तो
दिखे लेकिन जन चेतना और शिक्षा के मंतव्यों को व्यवस्थित ढंग से नियोजित करते हुए
व्यवस्था और विचारों के साम्य के लिए युवा धन निरंतर पैदा किया जाना विद्यालयीन
शिक्षा का मूल धेय्य होता है I धन बल और विवेक शुन्यता बालक के मन पर तामसी
प्रभावों का उन्नयन कर उसे नितांत असामाजिक और धेय्य विहीन बना देता है ; जिससे
उत्थान और पतन के बीच एक नकारात्मक विचार प्रक्रिया कीओर मुड जाता है I समय के
बदले चक्र में बाजारवाद और तकनीकी विस्फोट में युवा मन में शिक्षा के प्रति अलगाव
पैदा कर चुनौतियों की महंगी फसल खड़ी कर दी है I
आज एक और तकनीक से साम्य करने की आवश्यकता है
वहीँ दूसरी और विद्यालयों और शिक्षा केन्द्रों की महती आवश्यकता को पुनर्भाषित
करने की भी महती जरुरत है जिसे प्रारंभ में तकनीक बनाम शिक्षा के टकराव स्वरुप में देखा जा रहा था, जिससे पृथकतया
दोनों को एक दुसरे के प्रति सकारात्मक होकर परिवर्तित परिस्थितियों में समग्र रूप
से विद्यालयों को और व्यापक व विस्तृत विचार केंद्र के तौर पर रखना होगा जिससे
वैश्विक ज्ञान आवश्यकता की नयी परिपाटी गढ़ते , विद्यालय आज एक नवीन दौर में स्वयं
को सत्यापित कर सकें ,जिनकी आवश्यकता समाज को युगों से थी और रहेगी वरन बदले काल
क्रम में अधिकाधिक समायोजित और परिलक्षित रूप से व गुणवत्ता आधार पर यह और वांछनीय
है ; द्वापरयुग का निम्न उद्धरण उचित ही है –
“बालक कृष्ण युवराज तो हो सकते हैं
......किन्तु बिना गुरुकुलीय शिक्षा के चन्द्रवंशीय राजा कहलाकर भी अधूरे रहेंगे .....इसलिए
...वासुदेव दोनों की गुरुकुलीय (विद्यालयीन) शिक्षा सुनिश्चित करें.....”
आलेख द्वारा अमित तिवारी ; सहायक प्राध्यापक- पर्यटन प्रबन्ध
भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संसथान ,
ग्वालियर म.
प्र.
(पर्यटन मंत्रालय के अधीन एक संगठन)
22.10.2020
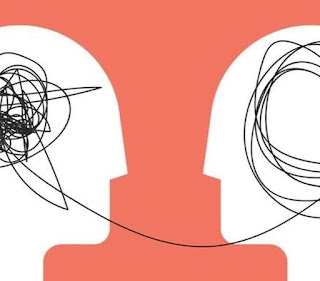

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें